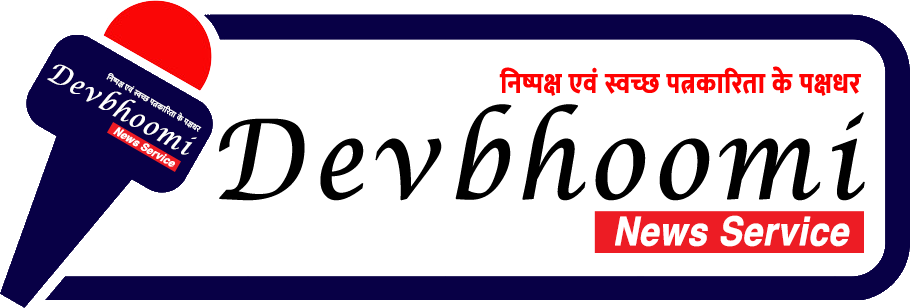नैनीताल वरिष्ठ पत्रकार प्रयाग पांडे
पर्यावरण प्रदूषण के चलते आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न संकटों से जूझ रही है। इस संकट से उबरने के लिए वैज्ञानिक उपाय खोजे जा रहे हैं। पर्यावरण को लेकर सदियों पुराने भारतीय दर्शन को नजरअंदाज किया जा रहा है। जबकि पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जैव विविधता के संरक्षण और संवर्धन का दार्शनिक पक्ष भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों में सदियों पहले से सम्मलित है।
प्रकृति और पारिस्थितिकी को लेकर भारतीय चिंतन सृष्टि के सिद्धांतों से प्रेरित है। भारतीय संस्कृति में पर्यावरण की कल्पना किसी निर्जीव भौतिक तत्व से नहीं की गई है। जीवित प्राणी की ही भाँति भौतिक पर्यावरण को भी जीवित संसार माना गया है। मानव और गैर मानव के बीच परस्पर आदान-प्रदान और सामंजस्य को तरज़ीह दी गई है। इन दोनों के संबंधों को जीवन का महत्वपूर्ण सिद्धांत माना गया है।
भारतीय दर्शन मानता है कि विश्व के प्रत्येक तत्व, वस्तु और जीव की सृष्टि एक ही परमात्मा ने की है। भारतीय दर्शन मनुष्य का प्रकृति पर कोई विशेषाधिकार को स्वीकार नहीं करता है। चूंकि मनुष्य ने इस प्रकृति का निर्माण नहीं किया है। मनुष्य पृथ्वी पर मौजूद समस्त भौतिक और प्राणिजगत का एक छोटा-सा अंश है। मनुष्य पृथ्वी का एक हिस्सा है, उसका स्वामी नहीं है। भारतीय दार्शनिक ग्रंथों में भी अजैविक संसार की कल्पना प्राणी से की गई है। इसे मानव के समान दर्जा दिया गया है और आत्मा का निवास स्थल माना गया है।
भारतीय चिंतन पर्यावरण को जैविक अथवा अजैविक पदार्थों का प्राणतत्व मानता है। भारतीय दर्शन में पर्यावरण और मानव जाति के बीच परस्पर सहयोग और निर्भरता को आवश्यक माना गया है। कहा गया है कि पर्यावरण के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार में ही मनुष्य का अस्तित्व निर्भर है। चूंकि पर्यावरण के बगैर अकेले मनुष्य के जिंदा रह पाने की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। पर्यावरण द्वारा समस्त मानव जाति की सभी आवश्यक आवश्यकताएं पूरी हो सकें इसके लिए पर्यावरण के साथ मित्रतापूर्ण रिश्ते और सहभागी जीवन का होना जरूरी है। चूंकि प्रकृति मनुष्य के वश में नहीं है, बल्कि मनुष्य प्रकृति के अधीन है।
विश्व के सभी प्रमुख धर्मों में प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की बात कही गई है। कहा गया है कि प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं, लिहाजा इनके संरक्षण और संवर्धन की आवश्यकता बताई गई है। विश्व की अनेक संस्कृतियों में भी पर्यावरण की कल्पना एक जीव के रूप में की गई है। पर्यावरण को मानव का मित्र और रक्षक बताया गया है।
माना जाता है कि वनस्पति समूहों के कारण ही मनुष्य का अस्तित्व संभव है। भारतीय दर्शन मनुष्य का प्रकृति और पशुओं पर प्रभुत्व और दमन के रिश्तों को भी मान्यता नहीं देता है। इनके बीच परस्पर आदर और दया का रिश्ता बताया गया है। पारिस्थितिकी और जैव विविधता को कायम रखने के लिए भारतीय संस्कृति में विभिन्न प्रजाति की वनस्पतियों, वृक्षों और जंगली एवं पालतू पशुओं की पूजा करने की परंपरा है। भारतीय दर्शन में कण-कण में ईश्वर की कल्पना की गई है।
भारतीय घरों में वृक्षों का विशेष स्थान है। वनों को ईश्वर तुल्य सम्मान दिया गया है। धार्मिक अनुष्ठानों में विभिन्न प्रजातियों के वृक्षों और अनेक वनस्पतियों का उपयोग किया जाता है। इनकी पूजा की जाती है। विभिन्न प्रजाति के वृक्षों को विभिन्न देवी-देवताओं के निवास स्थल के रूप में मान्यता मिली हुई है।
पुराणों में स्वर्ग प्राप्ति के लिए वृक्षारोपण की पैरोकारी की गई है। एक वृक्ष को दस पुत्रों के समान माना गया है। पुराणों में वृक्ष महोत्सव का उल्लेख मिलता है।वृक्ष की तुलना भगवान ब्रह्मा जी से की गई है। तुलसी, पीपल, वट, पदम और बेल आदि वृक्षों को अनेक देवी-देवताओं का निवास माना गया है। धार्मिक स्थलों और जल स्रोतों के आसपास पेड़ लगाने की परंपरा रही है। पर्यावरण संतुलन को कायम रखने के लिए उपयोगी विभिन्न पशु-पक्षियों को अलग-अलग देवी-देवताओं का वाहन बताया गया है। पशु-पक्षियों का मानवीकरण किया गया है। ताकि इनको संरक्षित किया जा सके।
कैलाश पर्वत को भगवान शिव जी का निवास स्थल माना गया है। शिव जी पहले पर्यावरण प्रेमी और संरक्षक हैं। वे पशुपति नाथ हैं। बेजुबान पशुओं को उनका संरक्षण प्राप्त है। शिव जी ने नंदी बैल को अपना वाहन बनाया है और सांड को संरक्षण प्रदान किया है। विषधर नाग उनका आभूषण है। शिव जी ने सांपों को अपना आभूषण बनाकर उन्हें अभयदान दिया है।
हिन्दू पौराणिक ग्रंथों में बुद्धि और ज्ञान के देवता श्रीगणेश जी का वाहन चूहा बताया गया है। शेर माता दुर्गा का वाहन है। देवी लक्ष्मी का वाहन उल्लू और सरस्वती का वाहन सफेद हंस है। शिवपुत्र कार्तिकेय मोर पर सवार हैं। क्षीर सागर में विराजमान भगवान विष्णु के वाहन पक्षीराज गरुड़ हैं। शेषनाग को उन्होंने अपनी शय्या बनाया हुआ है। इंद्र देवता का वाहन हाथी है। यमराज भैंसे पर सवार हैं। जबकि भगवान नरसिंह, आधे मानव और आधे सिंह के रूप में दिखाए गए हैं।
दुर्गासप्तशती के देवी कवच में वाराही देवी भैंसे की सवारी करती हैं। ऐन्द्री का वाहन हाथी है। वैष्णवी देवी गरुड़ में और माहेश्वरी वृषभ में विराजमान हैं। कौमारी देवी का वाहन मयूर है। लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजमान हैं। ब्राह्मी देवी का वाहन हंस है। वारुणी देवी मृग की सवारी करती हैं। जबकि चामुण्डा देवी प्रेत पर आरूढ़ हैं। भगवान कृष्ण गायों की सेवा और रक्षा के लिए स्वयं ग्वाले बन जाते हैं। भारतीय धर्म ग्रंथों में गाय की पूजा करने का विधान है। अग्नि को ईश्वर का दूत माना गया है। पृथ्वी को मातृ देवी कहा गया है। आकाश को पिता के रूप में पूजा जाता है।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वृक्षों और वनस्पतियों में ही नवग्रह विद्यमान हैं। नवग्रहों के पूजन में सूर्य के लिए आंक, चंद्रमा के लिए ढांक, मंगल के लिए खैर, बुध के लिए अपामार्ग, वृहस्पति के लिए पीपल, शुक्र के लिए गुलर (अमरूद), शनि के लिए शमि, राहू के लिए दुर्वा और केतु के लिए कुशा की समिधा उपयोग में लाई जाती है।
भारतीय दर्शन के अनुसार बुद्धि संपन्न होने के कारण पर्यावरण का संरक्षण करना मनुष्य का मूल कर्तव्य है। भारत के संविधान के अनुच्छेद- 51क (छः) में प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा को भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्य में शामिल किया गया है। संविधान में कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह- प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव हैं,रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणि-मात्र के प्रति दया भाव रखे। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में भी भूमि,जल और वायु प्रदूषण संबंधी अपराधों को रोकने के अनेक प्रावधान हैं।
हालांकि प्रकृति में प्राकृतिक रूप से बदलाव की एक सतत प्रक्रिया पिछले लाखों सालों से निरंतर चल रही है। प्राकृतिक बदलावों की गति बहुत धीमी होती है। प्रकृति की संवेदनशीलता को अनदेखा कर मनुष्यकृत विवेकहीन विकास ने इस रफ़्तार को कई गुना बढ़ा दिया है। जिससे समूचा प्राकृतिक ताना- बाना छिन्न – भिन्न होने की कगार पर आ पहुँचा है। नदियां, झरने, झील, वन और पहाड़ पर्यावरण के लिहाज से बेहद नाजुक माने जाते हैं। आज सबसे अधिक खतरा इन्हीं पर मंडरा रहा है।
यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रकृति पूर्वजों से हासिल पैतृक संपत्ति नहीं है। प्रकृति का पैतृक संपत्ति के रूप में लंबे समय तक निरंकुश दोहन नहीं किया जा सकता है। पर्यावरण के दीर्घकालिक संरक्षण के लिए समस्त प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन और दोहन के बीच उचित संतुलन कायम किया जाना बहुत जरूरी है। मानव जिसे सृजित नहीं कर सकता है, मानव को उसे नष्ट करने का अधिकार भी नहीं है।